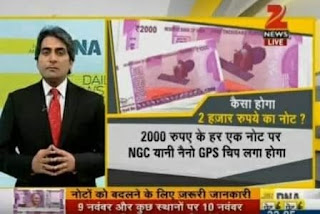||वीरान होते गांव||
गांवों से कुटीर उद्योग रवत्म हो गए हैं। पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। कुएं सूरव गए हैं और जो बचे हैं वे सूरवने के कगार पर हैं। ताल, पोरवर, बावड़िया, छोटी नदियां और नहरें सभी अपना अस्तित्व रखोती जा रही हैं या रखो चुकी हैं। लारवों गांवों में पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। मवेशी मर रहे हैं और रवेती सूरव रही है। गर्मी का बढ़ता प्रकोप जिंदगी को बदहाल कर दिया है.
हाल में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि अमेरिकी लोग शहरों की अपेक्षा गांवों में रहना अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण गांव की आबोहवा, शांति, सौहार्द और स्वतंत्रता के साथ जीने का आनंद बताया गया है। भारत में तो इसके ठीक उल्टा हो रहा है। लोग गांवों से पलायन करके कस्बों या शहरों में बसना अधिक पसंद करने लगे हैं। अमेरिका में हो रहे इस बदलाव की वजहें ऐसी नहीं हैं कि वह अविश्वसनीय लगें, क्योंकि वह ऐसा देश है जहां सुख-सुविधाओं की अपेक्षा अब लोग शांति, आंतरिक सुख और प्रदूषण रहित लोग शांति, आंतरिक सुख और प्रदूषण रहित माहौल को पसंद करने वाले हैं। जब कि अभी तक यही माना जाता रहा है कि शहर की सुख-सुविधाओं और आय के बेहतर साधनों को छोड़ लोग गांव में नहीं रहना चाहते। भारत में गांव पिछड़ेपन की निशानी हैं तो अमेरीकी में शांति और आनंद के धाम। अनेक विकसित देशों के सरकारी और निजी मुलाजिम भी गांवों में रहना अधिक पसंद करने लगे हैं। यानी विकसित देशों में भी शहर बदहाल होते जा रहे हैं। भारत के गांवों में न तो सरकारी चिकित्सक अपनी सेवा देना चाहते हैं और न ही दूसरे कर्मचारी। केंद्र सरकार ने पहली नियुक्ति के तहत चिकित्सकों को कुछ साल तक गांवों में सेवा देना अनिवार्य तो कर दिया, अब भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। आज भी गांवों की स्थिति दयनीय है। जो गांव भारत के गौरव, पहचान और अस्मिता के प्रतीक हुआ करते थे वे भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के प्रभाव के चलते अपने गौरव और पहचान को खोते जा रहे हैं।
ग्राम्य संस्कृति, कला, शिक्षा, व्यवहार और आचार-विचार की जो अहमियत कभी हुआ करती थी, वह अब बाजारीकरण और शहरीकरण के चपेट में आकर अपनी अहमियत खो चुके हैं और जो बचे हैं वे भी खोते जा रहे हैं। गांवों की लोक संस्कृति, लोक कलाओं, लोक शिक्षा, लोक धर्म और लोक भाषा कभी भारत की पहचान हुआ करती थे। भारत को समझने के लिए इन लोक प्रवृतियों को सबसे पहले समझना जरूरी होता था। इनकी अहमियत शहरी और नगरीय संस्कृति में पले-पढ़े लोग भी किया करते थेगांधी, विनोबा, लोहिया, जेपी, लालबहादुर शास्त्री, चौधरी चरणसिंह जैसे स्वदेशी के हिमायती लोगों ने गांवों के बढ़ने में ही भारत के बढ़ने के सूत्र देखते थे। इसलिए गांधी और लोहिया गांवों के कुटीर उद्योग, ग्राम्य-शिक्षा, ग्राम्य-संस्कृति, शाकाहार-संस्कृति और ग्राम्य-कलाओं को संरक्षित करके आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी मानते थे।
आज भी गांव विकास की प्राथमिकता की सूची में नहीं हैं। शहर की छांव तले जितने भी गांव हुआ करते थे वे सभी अब शहर के हिस्से होते जा रहे हैं और वहां भी एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। नाम तो आज भी इनका वही पुराना गांव का ही है लेकिन वहां गांव दूर-दूर तक नहीं हैं। नई मोदी सरकार गांव, गाय, गंगा और गौवंष की हिाजत करने की बात कर रही हैगांव की बदहाली को जो समझता है वही गांव और गांव की सभी प्रकार की प्रवृतियों को समझ सकता है।
गांवों से कुटीर उद्योग खत्म हो गए हैं। पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। कुएं सूख गए हैं और जो बचे हैं वे सूखने के कगार पर हैं। ताल, पोखर, बावड़िया, छोटी नदियां और नहरें सभी अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं या खो चुकी हैं। लाखों गांवों में पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। मवेशी मर रहे हैं और खेती सूख रही है। गर्मी का बढ़ता प्रकोप जिंदगी को बदहाल कर दिया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु जैसे अनेक राज्यों की हालात अत्यंत भयावह होती जा रही है। कहीं सूखे ने बदहाल किया है तो कहीं बरसात ने। कहीं तूफान ने तो कहीं बाढ़ ने। गांवों से बदहाली के चलते लगातार पलायन जारी है.
गांव जिन संसाधनों और लोक प्रवृतियों से संपन्न हुआ करते थे आज वे दिखते नहीं हैं। गांवों में जो समरसता, भाईचारा था, वहां बाजार आकर खड़ा हो गया है। सारे रिश्ते, बाजार से तय होने लगे हैं। चौपाल में चलने वाली बैठकें, ठहाके, किस्से और लोकगीत नए बाजार के भेंट चढ़ गए हैं। गंवई सुख की जगह बाजारू तनाव लोगों के माथे पर सा देखा जा सकता है। बाजार ने गांव के हर व्यक्ति को आर्थिक प्रलोभन देकर अपने चंगुल में फंसा लिया है। गांवों के वाद्य-यंत्र, कलाकार, गीत और कहकहे अपसांस्कृतिक बाजारवाद के शिकार बनते जा रहे हैं।
आजादी के बाद सैकड़ों नए कस्बे और शहर अस्तित्व में आए मगर गांवों को बलि देकर। शहरों के पचास किलोमीटर तक के गांव आज शहरों की प्रदूषित हवा, अपसंस्कृति और बचकानेपन में खपते जा रहे हैं। इसे विकास का नाम दिया जा रहा हैगांवों से लोगों का पलायन शहरों की तरफ जितनी तेजी से पिछले पच्चीस वर्षों में हुआ, उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। गांवों में आज खेती सबसे उबाऊ कार्य है जिसे गांव का कोई नौजवान नहीं करना चाहता है। इसलिए वह रोजगार की तलाश में शहर की ओर भागता है और कमरतोड़ मेहनत के बाद भी उसी बदहाली में रहने के लिए अभिशप्त है। खेती करना पिछड़ेपन की निशानी हो गई है। हिंदी या उसकी मातृभाषा अब उसके लिए हीनभावना का सबब बनती जा रही है।
यह सब बाजारी विज्ञापनों का असर है जिसे धीमे जहर की तरह गांव के प्रत्येक व्यक्ति की नस-नस में अखबारों, टीवी सीरियलों और फिल्मों के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत चालाकी और योजनाबद्ध तरीके से मीडिया के जरिए भारत के गांवों को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, उसका असर पूरी तरह से दिखाई पड़ने लगा है।
भारत के किसी भी गांव में चले जाइए, वहां अब सिर्फ बूढ़े, कुछ बच्चे और परेशानहाल महिलाएं ही बच गई हैं। बाकी सब शहर चले गए हैं नौकरी करने या किसी अन्य काम से। कुछ दिखाई पड़ता है तो वह बाजार और केवल बाजार। बाजार की विडंबना और संवदेनहीनता, जिसे विकास का नाम देकर आगे बढ़ाया जा रहा है।