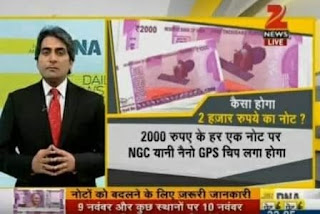||राजनीति दही में जमण का कार्य करती है||
एक बड़ी चुनौती ये भी है कि कैसे आम पर्वतीय परिवार यहाँ रहकर अपने को ठीक से ससम्मान टिकाये। यद्यपि बहुत से लोगों ने इसके उपाय खोजे भी हैं। व्यक्तिगत रूप में उन्होंने अपनी आजीविका को बढ़ाया भी है। लेकिन यकीनन उनके पास कुछ संसाधन पिछली पीढ़ी के थे या परम्परागत रहे हैं।
आम व्यक्ति ऐसे जीवन यापन का उपाय नहीं कर सकता। उपर से पर्वतीय जमीनों के पुश्तैनी विभाजन इतने तनाव देने वाले हैं कि जो मौजूदा भूमि और अन्य व्यवस्थाएं हैं वे बिना सरकारी तन्त्र में पड़े समझ में ही नहीं आती। उलझनें देखकर ही काफी लोगों ने गाँव का बड़ा सा घर छोड़कर किसी शहर में घर बनाया है। क्योंकि एक बड़े से घर में जितने भागीदार होते हैं उससे आपस में सिर्फ झगड़ा हो सकता है। वैसे ही साझी विरासत की जमीनें भी अब मात्रा में कम रह गयी और अपने साथ झगड़ा जरुर पैदा कर लेती हैं। इसमें गाँव की कुटिल ईर्ष्यालु राजनीति दही में जमण का कार्य करती है। तब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या किया जाना चाहिए?
उत्तराखंड बनते समय से आज तक हम लगातार हिमाचल की भूमि व्यवस्था का राग सुनते हैं। हम ये भी सुनते हैं कि वहाँ की सरकार ने वृक्ष खेती को विशेष महत्व दिया है। सरकार के पास उस प्रबन्धन के सही उपायों की जानकारी भी है। फिर ये कैसी नालायकी है जिससे राज्य की आर्थिकी और समाज की व्यवस्था पर ही संकट खड़ा हो गया है।
अब भूमि का बेहतर प्रबन्धन लोगों के आलावा किसके हित में हो सकता है? दूसरा बड़ा कार्य पटवारी व्यवस्था,ग्रामीण बैंकों के संचालन और ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण की दिक्कतों को सहज बनाने का है। यहाँ जो बाहर से आये भूमि के सौदागर हैं उनको सरकार प्रदत्त सभी सुविधाएँ आसानी से मिल जाती हैं और स्थानीय गरीब बागवान किसान भटकता रहता है। बैंकों का कर्ज भी अधिक फर्जी लोगों को सहजता से मिलता रहा है।
विधायक नेता अफसर भी आम पर्वतीय किसान के लिये खुदाई आवरण ओढ़े चलते हैं। उनके चंट मन्ट ही उनको ये बताते हैं कि उनको किस् व्यक्ति से मिलना फायदा देगा और किस समय क्या ड्रामा करना है? मूल मुद्दों से दूर ग्रामीण जन प्रतिनिधि मात्र सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सरल करते दिख रहे हैं। ये सब आम पहाड़ी न्यून भूमि पर बिना चकबंदी और बिना सिंचाई के खेती करके जीवन निर्वाह करते व्यक्ति के लिए अत्यधिक कष्ट देने वाला मामला बन गया है। जनप्रतिनिधि इसे सुलझाएं।